पैसा सब कुछ है …. पैसा सब कबाड़ा कर रहा है।
इस सन्दर्भ में मजदूर समाचार के नवम्बर 2010 अंक से “रुपये का उत्पादन और वितरण” प्रस्तुत है।

पैसा सब कुछ है …. पैसा सब कबाड़ा कर रहा है।
इस सन्दर्भ में मजदूर समाचार के नवम्बर 2010 अंक से “रुपये का उत्पादन और वितरण” प्रस्तुत है।
A Glimpse of Social Churnings
Attempts at conversational interactions during global Covid lockdowns.
47 pages booklet
A Majdoor Samachar
Kamunist Kranti presentation
September 2020
“मजदूर समाचार पुस्तिका तेरह” का आनन्द लें।
जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009
सम्भव है
कुछ प्रस्थान बिन्दु मिलें।
# आदान-प्रदान बढाने के लिये अपने ग्रुपों में फॉर्वर्ड करें।
# दिल्ली और इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति को देखते हुये अभी पुस्तिका छापेंगे नहीं। व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा इसे प्रसारित करेंगे। उपलब्ध अन्य माध्यमों द्वारा आदान-प्रदान बढाने में आप भी योगदान करें।
# आप स्वयं छापना चाहते हैं तो खुशी-खुशी छापें। ए-4 साइज के 43 पन्ने हैं।
# पढते समय जो त्रुटियाँ मिलें वो बताना ताकि छापने से पहले हम उन गलतियों को दूर कर सकें।
Read the full piece here: Fear of the unknown. Efforts of power to reestablish itself.
Read our contribution to internationalist communist summer meeting organized by TPTG, Underground Tunnel and friends from 11th to 17th July 2017 in Greece here :
“मजदूर समाचार पुस्तिका बारह” का आनन्द लें।
पहला पन्ना 2010 से 2015
सम्भव है
कुछ प्रस्थान बिन्दु मिलें।
# आदान-प्रदान बढाने के लिये अपने ग्रुपों में फॉर्वर्ड करें।
# दिल्ली और इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति को देखते हुये अभी पुस्तिका छापेंगे नहीं। व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा इसे प्रसारित करेंगे। उपलब्ध अन्य माध्यमों द्वारा आदान-प्रदान बढाने में आप भी योगदान करें।
# आप स्वयं छापना चाहते हैं तो खुशी-खुशी छापें। ए-4 साइज के 199 पन्ने हैं।
# पढते समय जो त्रुटियाँ मिलें वो बताना ताकि छापने से पहले हम उन गलतियों को दूर कर सकें।
“मजदूर समाचार पुस्तिका ग्यारह” का आनन्द लें।
जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010
सम्भव है
कुछ प्रस्थान बिन्दु मिलें।
# आदान-प्रदान बढाने के लिये अपने ग्रुपों में फॉर्वर्ड करें।
# दिल्ली और इर्द-गिर्द के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिति को देखते हुये अभी पुस्तिका छापेंगे नहीं। व्हाट्सएप और ईमेल द्वारा इसे प्रसारित करेंगे। उपलब्ध अन्य माध्यमों द्वारा आदान-प्रदान बढाने में आप भी योगदान करें।
# आप स्वयं छापना चाहते हैं तो खुशी-खुशी छापें। ए-4 साइज के 42 पन्ने हैं।
# पढते समय जो त्रुटियाँ मिलें वो बताना ताकि छापने से पहले हम उन गलतियों को दूर कर सकें।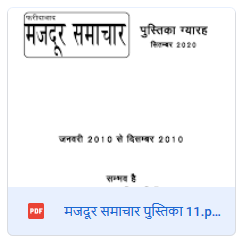
# चालाकी यह नहीं देखती कि सम्बन्धों का क्या हो रहा है।
# समझदारी सम्बन्धों को टूटने नहीं देती क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी काम आ सकते हैंं। काम चलाऊ सम्बन्ध। मधुर सम्बन्ध नहीं।
# चालाकी और समझदारी विगत में महाभारत लिये थी — बन्धुओं द्वारा परस्पर हत्यायें।
# आज चालाकी और समझदारी बहुत-ही व्यापक हैं। सामाजिक मनोरोगों का बोलबाला।
इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है मजदूर समाचार के दिसम्बर 2010 अंक से “चालाकी-समझदारी और सीधापन”।
## इन तीन सौ वर्षों के दौरान संसार-भर में निवासियों से जमीनें छीनने के अभियान।
## इस उपमहाद्वीप में 1824 में जमीन छीनने के लिये कानून बनाया गया। बदलते हुये यह 1894 का जमीन छीनने का कानून बना। भारत में ब्रिटिश सरकार के सीधे नियन्त्रण वाले क्षेत्रों में यह 1947 तक लागू रहा।
## रजवाड़ों को मिला कर बने उपमहाद्वीप के भारत क्षेत्र की सरकार ने जमीन छीनने के लिये 1894 में बने कानून को पूरे भारत में लागू कर दिया।
## जमीनें छीनने का 1894 का कानून जस का तस भारत सरकार ने 1947 से 2013 तक जारी रखा।
इस सन्दर्भ में मजदूर समाचार के अगस्त 2010 अंक से “ग्रामीण गरीबों के खिलाफ नया युद्ध” प्रस्तुत है।
#The communist movement in India is turning 100 years old in October this year, and here’s a publication from Tricontinental: Institute for Social Research on this occasion. The India office of the institute has taken the lead in producing this, with plenty of help from our colleagues at the other offices.
Many of those who know a fair deal about the communist movement in India would find that several important struggles, events, aspects and even organisations are missing in this story. But we had to keep it somewhat short, keeping in mind the usual size of our dossiers, even though the topic is vast. Nevertheless we hope this will be a useful overview. Even those who know about the movement very well might find it interesting to look at and to circulate among their friends, family and acquaintances.
Right now the dossier is available in English, Spanish and Portuguese. More translations are on the way, including in some Indian languages. Please do read and share.
The dossier has some nice, historic photographs as well. You’ll find a beautifully designed pdf copy available for free download if you scroll down to the end of the page. ????
## FMS: to rule with a General-Colonel Red Army. For most “Marxists” Marx is foreign.
Expansion of factory production engendered a social strata that self-characterised itself as “intellectuals”. With owner-based factories displacement by joint stock companies came managements. Dominant part of “the intellectuals” constitute managements in companies. A part of “the intellectuals” , revolutionary intellectuals constitute “Marxists”.
Karl Kautsky, a leading theoretician, formulated the framework of revolutionary intellectuals :
“1. Communist consciousness comes from the studies of philosophy, history, economics etc.
2. Wage-workers on their own can at most achieve trade union consciousness.
3. Communist consciousness needs to be injected in wage-workers from outside. Revolutionary intellectuals have to play this historical role.”
Lenin in his 1903 book, “What is to be done?” puts forward a popular version of Karl Kautsky’s theory. October 1917 catapulted Lenin on the global stage.
With the incomparable leap in productive forces premised on electronic machines, in the 1970s began the rapid transformation of universities into knowledge production factories. The irrelevance of “intellectuals” social strata in general and “revolutionary intellectuals” in particular is in front of us. This is nothing to lament about. Rather, these are vibrant-lively times to contribute to global radical transformations taking place all over the world.